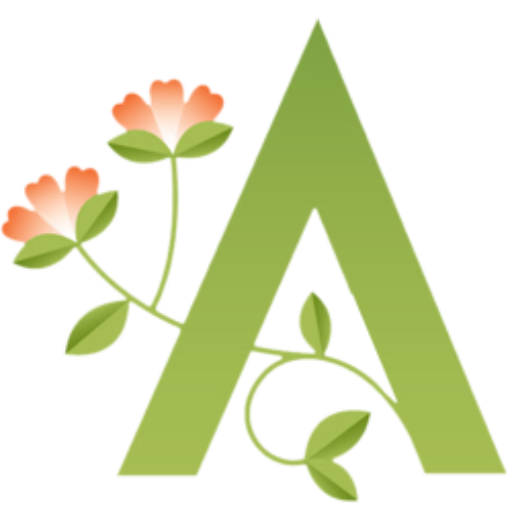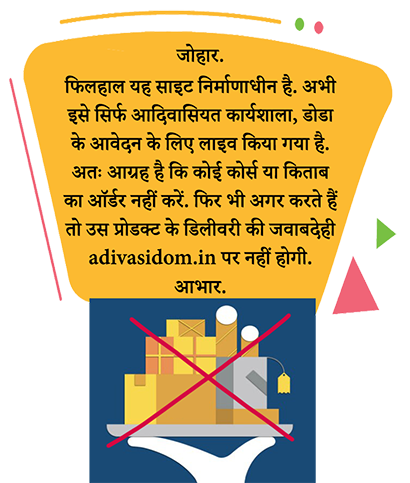आदिम समाजों की ज्ञान परंपरा
अनेक इतिहासकारों, मानवशास्त्रियों, समाजविज्ञानियों, भाषाविदों और विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि आज जिन्हें आदिम, कबिलाई अथवा आदिवासी समाज के रूप में चिन्हित किया जाता है, उन्होंने ही अपने श्रम और मेधा से मानव सभ्यता के नये युग की सुदृढ़ नींव डाली थी। मोहनजोदाड़ो-हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो यह स्पष्ट धारणा है कि इसके जनक मुुंडा आदिवासी समूह के आग्नेय लोग थे। बाद में जो जलवायु परिवर्तन या आर्यों की आक्रमणकारी घुसपैठ की वजह से घने जंगलों में रहने के लिए बाध्य हुए। वैदिक साहित्य में आर्यों और अनार्यों (आदिवासियों) के संघर्ष की अनेक कथाएं हैं जिनसे यह बात प्रमाणित होती है कि हड़प्पा के पराभव के बाद इन दोनों मानव समूहों के बीच निरंतर संघर्ष हुए। जिससे स्थायी रूप से उनकी आर्थिक संरचना बदल गई और उन्होंने कृषि-कार्य की अपेक्षा आहार-संग्रह, घुमंतू और अर्द्ध-कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था में जीने की प्रणाली विकसित की।
परंतु इसी के साथ एक और तथ्य है जिसकी ओर विद्वानों का ध्यान बहुत कम गया है। विकसित और अविकसित समुदाय, समाज और राष्ट्र का विभाजन मुख्यतः कृषि के विकास, तकनीक की प्रगति, परिवर्तनशील उत्पादन संबंध और इससे भी बढ़कर मनुष्य की असीमित आकांक्षाओं के कारण संभव हुआ। एक ने जहां प्रकृति के नियमों का अनुसरण किया, वहीं दूसरे में उस पर विजय पाने की लालसा बढ़ती गई। नागर समाज और वन्यजीवी समाज के बीच यह ‘व्यक्तिगत’ आकांक्षा अथवा लालसा ही मुख्य विभेद है। इसी विभेद के कारण विकास की आधुनिक सदी और पूरवर्ती सदियों में भी दोनों के बीच लगातार टकराव होता रहा है। यह टकराव आज भी जारी है और 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके मानव समुदायों में भी यह विभेद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।
विकास को लेकर दोनों के बीच दो तरह की अवधारणाएं हैं और ये दोनों मानव समाज जिनमें से एक को भारत में ट्राइबल, आदिवासी या अनुसूचित जनजाति और वैश्विक स्तर पर इंडीजीनस कहा जाता है, और दूसरे को आर्यन अथवा गैर-आदिवासी के रूप में जाना जाता है, विकास संबंधी अपनी-अपनी अवधारणाओं के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई व आर्थिक संरचना के दो छोरों पर खड़े हैं। यानी एक विकसित समाज है तो दूसरा अविकसित और पिछड़ा समाज है। इस संबंध में भी बौद्धिक और अकादमिक जगत में दो तरह की अवधारणाएं प्रचलित हैं। पहली अवधारणा तथाकथित रूप से विकसित यूरोपीय देशों की है जबकि दूसरी अवधारणा भारत जैसे पिछड़े और अविकसित राष्ट्रों की है।
विकसित एवं सभ्य कहे जाने वाले नागर समाज के प्रतिनिधियों ने लंबे समय तक दुनिया के अधिकांश देशों के मानव समूहों को अपना उपनिवेश बनाए रखा और उनकी विकसित ज्ञान व शिक्षण परंपरा को अस्वीकार किया। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणालियों के द्वारा उनकी ज्ञान परंपरा और पारंपरिक शिक्षण पद्धति को नष्ट कर देने की हरसंभव कोशिश की। अविकसित और पिछड़े कहे गए आदिम समाज में ज्ञान बांटने की अपनी शिक्षण प्रणाली थी। इस संदर्भ में इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं, ‘उन्नीसवीं शताब्दी में, जब यूरोप ने आधुनिक युग में प्रवेश किया तो यह रवैया बदलना शुरू हो गया, और कई क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति उत्साह प्रायः उसी अनुपात में कम हो गया जितना पहले उत्साह का अतिरेक था। अब यह पाया गया कि भारत में कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसकी नवीन यूरोप सराहना करता। विवेकयुक्त विचार और व्यक्तिवाद के मूल्यों पर स्पष्टतः यहां कोई बल नहीं था। भारत की संस्कृति गत्यवरुद्ध संस्कृति थी और इसे अत्यंत तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा। यह प्रवृत्ति भारतीय वस्तुओं के प्रति मैकाले के तिरस्कार में शायद सर्वोत्तम ढंग से मूर्तिमान हुई है।’5
अर्थात् जो सलूक आर्य घुसपैठियों ने वैदिक और पौराणिक काल में भारतीय भूमि के मूल आदि निवासियों के साथ की थी, उनकी संस्कृति और ज्ञान परंपराओं का जिस तरह से तिरस्कार और निषेध किया था, अंग्रेजों ने भी ठीक वही नस्लीय अपमान का उपनिवेशी रवैया भारतीय आर्यों के प्रति अपनाया। मैकाले ने अपने वक्तव्यों में इस उपनिवेशवादी नजरिए को गर्वपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करते हुए कहा है – ‘‘मैंने भारत के ओर-छोर का भ्रमण किया है और मैंने एक भी आदमी नहीं पाया, जो चोर हो। इस देश में ऐसी समृद्धि, ऐसे सक्षम व्यक्ति तथा ऐसी प्रतिभा देखी है कि मैं नहीं समझता कि हम इस देश को विजित कर लेंगे, जबतक कि हम इसके सांस्कृतिक एवं नैतिक मेरूदंड को तोड़ न दें। इसलिए मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि हम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति को बदल दें। क्योंकि यदि भारतवासी यह सोचने लगेंगे कि जो विदेशी एवं अंग्रेजी है, वह उनके आचार-विचार से अच्छा व बेहतर है, तो वे अपना आत्मसम्मान एवं संस्कृति खो देंगे और वे एक पराधीन कौम बन जाएंगे, जो हमारी चाहत है।’’ (लार्ड मैकाले का 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में दिए गए वक्तव्य का अंश)
यह सही है कि विकसित समाजों अर्थात् लिखित नागर समाजों ने आदिम और पिछड़े समाजों के मौखिक ज्ञान परंपरा, इतिहास आदि का दस्तावेजीकरण किया। मौखक परंपरा में जीवित आदिवासियों की भाषा-संस्कृति, ज्ञान परंपरा और उनके वाचिक साहित्य को संकलित-संग्रहित कर उसे लिखित रूप दिया। जिससे दुनिया आदिवासियों की भाषा-संस्कृति, ज्ञान और वाचिक साहित्य से परिचित हो पाई। लोग यह जान सके कि जिन्हें आदिम और पिछड़ा कहा जा रहा है वे तो विकसित माने जाने वाली सभ्यताओं से बहुत आगे हैं। यही नहीं, दुनिया के तमाम विकसित समाज उसी ज्ञान परंपरा का अनुसरण करते हुए सभ्यता-संस्कृति के आज की मंजिल तक पहुंच पाने में सफल हुए हैं।
आदिवासी वाचिक लोक साहित्य के विद्वान जगदीश त्रिगुणायत ने अपनी पुस्तक ‘मुंडा लोक कथाएं’ में आदिम समाजों के ऐतिहासिक अवदानों पर संक्षेप में, किंतु सारगर्भित ढंग से यथेष्ट प्रकाश डालते हुए लिखा है- ‘‘भारतीय महादेश में बहुत पहले आने वाली और द्रविड़-आर्यों के आगमन के पहले की लंबी अवधि में ही एक समृद्धशाली सभ्यता का निर्माण करनेवाली इस आग्नेय जाति ने स्वभावतः ही भारतीय सभ्यता को बहुत कुछ दिया है। अनेक वानस्पतिक पदार्थ, कृषि, अनेक अविष्कार, विविध वस्तुओं के नाम आदि के स्थूल क्षेत्रों, और विचारों, देव-कल्पनाओं और धार्मिक धारणाओं के अपेक्षया सूक्ष्मतर क्षेत्रों, दोनों में भारतीय संस्कृति में आदिमजातियों के प्रभाव की खोज हो चुकी है।…नये अनुसंधान इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि अब आईने में नहीं, एक्स-रे में अपनी छवि देखो–तुम्हारे रक्त, मांस, मज्जा यहां तक कि विचार और भावना में भी आदिवासी मौजूद हैं।’’6
आगे जगदीश त्रिगुणायत अत्यंत प्रखर ढंग से आदिवासियों के महत्वपूर्ण अवदानों की चर्चा करते हैं –
- ‘‘आग्नेय जातियों ने ही भारत में झूम-कृषि की प्रणाली चलाई। और पहले पहल धान की खेती शुरू की।
- केला और नारियल, पान और सुपारी, हल्दी और अदरख, लौकी, बैगन तथा काशीफल उन्होंने ही उपजाये।
- कपास का वस्त्रा सबसे पहले उन्होंने ही बनाया।
- जंगलों से पकड़कर मुर्गी को उन्होंने ही पाली और विशाल जानवर हाथी को सबसे पहले उन्होंने ही पालतू बनाया।
- हल और उसकी यह संक्षा उन्हीं की देन है।
- पतित-पावनी ‘गंगा’ का यह पवित्रा नाम उन्हीं के शब्द भंडार का है।
- हिन्दू नारियों का सुहाग चिन्ह सिन्दूर उन्होंने ही सभ्यता को दिया है।
- कहते हैं, इन्हीं आग्नेयों ने बीज और वृक्ष के संयोजन-वियोजन के क्रमों को देखकर पुनर्जन्म (पूर्व या पुरखा आत्माओं) की कल्पना की। आर्य मूलतः इससे अनभिज्ञ थे।
- चन्द्रमा को देखकर तिथि-गणना का रिवाज आग्नेय सभ्यता की ही देन है। पूर्ण चन्द्र के लिए ‘राका’ और नये चन्द्र के लिए ‘कुहू’ शब्द आग्नेय भंडार से ही आये हैं।
- मुर्दे की राख के जल-प्रवाह का प्रचलन, आरंभ में आग्नेय जातियों से ही लिया गया है।
- वृक्षों और नदियों की पूजा, पत्थर के टुकड़ों की पूजा, ग्राम-देवता, डीह और वरम् आदि आदिमजातियों से लिये गये हैं।
- टोटेम से बनी हुई गोत्र-प्रणाली का अविष्कार करने वाले आदिवासी ही हैं।
- बीस-बीस करके (कोड़ी के अनुसार) गिनने की प्रणाली, मनुष्य की बीस उंगलियों के अनुसार आग्नेयों ने ही निकाली है।
- भारतीय भाषाओं को अनेक संज्ञायें आग्नेय भाषाओं की देन हैं।
- भाषाशास्त्रियों ने संस्कृत के साढ़े चार सौ के लगभग ऐसे शब्दों को खोज निकाला है, जिनका आर्येतर (आग्नेय) स्रोत हैं।’’ 7
यही नहीं, आर्यों ने वैदिक समय में जिस शिक्षण परंपरा के शुरुआत की सुदृढ़ नींव डाली, उसे भी आदिम समाजों से ही लिया गया है।
‘नालंदा’ और ‘तक्षशिला’ जैसे जिन विश्वविख्यात प्राचीन विश्वविद्यालयों का इतिहास हमें बताया जाता है, इसकी पूरी संकल्पना आदिवासियों के मौखिक विश्वविद्यालयों, यथा- गीतिओड़ा, धुमकुड़िया, जोंख एड़पा, घोटुल आदि के आधार पर की गई थी। ‘गुरु-शिष्य’ की श्रुति परंपरा आदिवासियों के लोकशिक्षण की मौखिक परंपराओं का ही विस्तार है जहां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने अनुभवों व ज्ञान का हस्तांतरण करती थी। आदिवासियों से ली गई शिक्षण-प्रणाली के आधार पर गेय-श्रुति परंपरा का विकास हुआ और दुनिया के सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथों -वेदों की रचना संभव हो सकी।
स्पष्ट है कि आज जो भारतीय सभ्यता-संस्कृति की विशाल और समृद्धशाली इमारत हमें दिखाई पड़ती है, उसके मूल में आदिम निवासियों का ज्ञान और शिक्षण परंपरा ही है जिसे आगे चलकर आर्यों ने अपनी संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के अनुरूप ढाला तथा विकसित किया।
इस तथ्य को रेखांकित करते हुए सुप्रसिद्ध विद्धान डॉ. भगवान सिंह, जिन्होंने हड़प्पा और वैदिक सभ्यता-संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, लिखते हैं, ‘‘भारतीय सभ्यता हजारों साल की लंबी यात्रा करते हुए वहां तक पहुंची थी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं। इसका निर्माण किन तत्वों से हुआ था, इसके विकास में कितना लंबा समय लगा था, और इस क्रम में भारतीय समाज को किन अनुभवों से गुजरना पड़ा था, इसकी तलाश कभी गंभीरता से नहीं की गई। … उस महायात्रा पर पुरातत्व से भी उतना स्वच्छ प्रकाश नहीं पड़ता जितना इन (भाषिक) स्रोतों से। पुरातत्व सहित इन सभी स्रोतों को जोड़ कर हड़प्पा का एक लम्बा विवरण तैयार किया जा सकता है। … भारतीय सभ्यता का आरंभ हड़प्पा सभ्यता से नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता विकासयात्रा में एक बीच का चरण है।’’8
अतः ऐतिहासिक तथ्यों के अवलोकन एवं उनके विश्लेषणात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे समाज एवं राजनीति में ‘व्यक्ति आधारित स्वार्थ’ बढ़ता गया वैसे-वैसे देशज ज्ञान परंपरा का निषेध किया जाने लगा जो उच्चतर मानवीय मूल्यों व जीवन-दर्शन के पक्षधर थीं। इसीलिए नगरों एवं राज्यों के उदय के बाद, वैदिक काल से लेकर अब तक न सिर्फ आदिवासी समाजों की ज्ञान परंपरा को विस्मृत करने का हरसंभव प्रयास हुआ, बल्कि एक ऐसी शिक्षण-प्रणाली भी विकसित की गई जो एकांगी थी। अंग्रेजों के आगमन से पहले यह काम आर्यों ने वेद, पुराण, ब्राह्मण और रामायण-महाभारत जैसे ग्रंथों तथा ‘गुरुकुल आश्रम’ वाली शिक्षा प्रणाली के द्वारा किया तो ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक स्कूली शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रमों के जरिए अंग्रेजों ने उसे अंजाम दिया। आदिम एवं पिछड़े समाजों के बारे में नस्लीय भेदभाव, हीनता व घृणा के बीज बोये। चिंताजनक विषय है कि 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी दुनिया में भी आदिम एवं पिछड़े जनों के बारे में भी इस तरह की धारणा और दृष्टि बरकरार है।
पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरह से प्राचीन भारत में दो तरह के सामाजिक संरचनाओं का क्रमिक ढंग से विकास हुआ, उसी के अनुरूप दो तरह की ज्ञान एवं शिक्षण प्रणालियां भी अस्तित्व में आईं। आदिम जनों ने अपनी सामाजिक संरचना को अविच्छिन्न रूप से जारी रखने के लिए पंरपरा की रक्षा पर विशेष बल दिया, और इसी के अनुरूप लोकशिक्षण की मौखिक पद्धति का सूत्रपात किया तथा उसे स्थायित्व प्रदान किया। आदिम समाजों के लोकशिक्षण की इस परंपरा में सामूहिक रूप से समूचा समुदाय ‘गुरु’ और पूरा गांव-परिवेश ‘गुरुकुल’ होता था, जो सहभागी शिक्षण की विधि से एक ही समय में स्वयं को भी, और अपनी नई पीढ़ी को भी, एक साथ शिक्षित-प्रशिक्षित करता था। सीखने-सिखाने की यह अद्भुत, अनूठी और प्रभावी शिक्षण प्रणाली थी जिसमें पुराना नये को ज्ञान तो सौंपता ही था, वह नये से भी सीखता था। जबकि गैर-आदिवासी आर्य शिक्षण परंपरा ‘गुरुकुल’ आधारित थी जो गांव-समाज से दूर निर्जन वन-प्रांत में किसी एक गुरु के अधीन रहकर विद्या प्रदान करने का कार्य करती थी। पर आदिम शिक्षण विधि ‘गुरु-शिष्य’ परंपरा और न ही आज की स्कूली ‘कान्वेंट’ शिक्षा की तरह ‘वन-वे’ थी। बल्कि वह शिक्षण की दोतरफा प्रक्रिया थी जिसमें सीखने और सिखाने वाले के बीच किसी भी किस्म का ब्राह्मणवादी विभाजन नहीं था। यह नजरिया हम आदिवासियों के दूसरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवहारों में भी देख सकते हैं। जैसे उनके सांस्कृतिक स्थल ‘अखड़ा’ में कलाकार और दर्शक का भेद नहीं रहता। अखड़ा में हर व्यक्ति कलाकार भी है और दर्शक भी। खेती-किसानी के कार्यों, वन उत्पादों एवं आहार संग्रह, शिकार आदि में भी उनका सहभागी क्रियाकलाप रहता है। इस संबंध में दिलचस्प तथ्य यह है कि आज जब जड़ और औपनिवेशिक स्कूली शिक्षा प्रणाली, उसकी व्यावहारिक उपयोगिता, गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसके जबाव में विश्व स्तर पर शिक्षा की नई प्रविधियों के अंतर्गत आदिम लोकशिक्षण परंपरा को ही अपनाया जा रहा है। और यह भी कि इसे भी पूर्व की तरह ही नागर समाज के शिक्षाविदों की व्यक्तिगत क्रांतिकारी देन बताया जा रहा है।
संदर्भ:
- रोमिला थापर, भारत का इतिहास, पृष्ठ-11-12
- जगदीश त्रिगुणायत, मुण्डा लोक कथाएं, पृष्ठ-33
- वही, पृष्ठ-34-36
- भगवान सिंह, भारतीय सभ्यता की निर्मिति, पृष्ठ-24-25