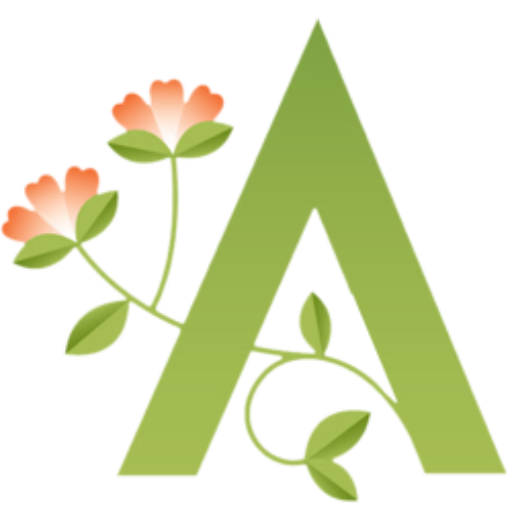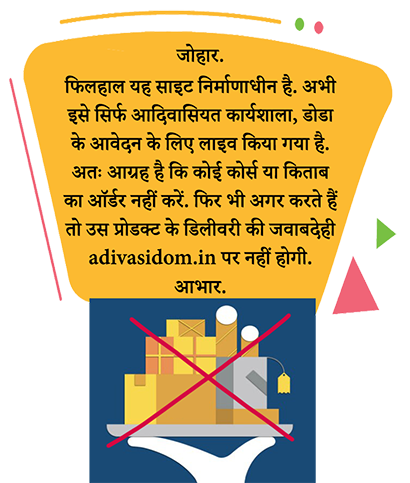ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा का मर्म
ब्रिटिश औपनिवेशिक ‘‘शिक्षा की व्यापकतर प्रणाली ने लोगों के ज्ञान और चिंतन तथा कर्म की उन पद्धतियों को मान्यता देने से इंकार कर दिया जो यहां के सांस्कृतिक ढांचे के तहत सम्माननीय मानी जाती थीं। औपनिवेशिक शासन ने सामान्य स्कूलों की पाठ्यचर्चा में देशज ज्ञान और सांस्कृतिक रूपों को शामिल करने की किसी भी संभावना की जगह नहीं छोड़ी। उपनिवेशवाद की सांस्कृतिक भूमिका, जिसका विकास 19वीं सदी के प्रारंभ से होना शुरू हुआ, इस नजरिए पर टिकी हुई थी कि देसी ज्ञान और संस्कृति में ‘खामियां’ हैं। भारत की भौतिक कंगाली को उन ढेरों कमजोरियों के प्रमाण के रूप में देखा गया, जिनसे भारतीय संस्कृति पीड़ित समझी जाती थी। नैतिक और भौतिक सुधार के एक साधन के रूप में शिक्षा संभवतः खामियों भरी एक संस्कृति को अपने ज्ञानमीमांसीय आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती थी; उसकी जड़ें उस ज्ञान और संस्कृति में ही धंसी रहनी थीं जो उपनिवेश की प्रतिनिधि थीं।’’1
हालांकि ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली की तुलना में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की परियोजना उदार थी। उनकी शिक्षा प्रणाली हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच प्रचलित शिक्षा से भिन्न और एक प्रकार से उन्नत भी थी, जिसके कारण आगे चल कर शिक्षा पर जाति विशेष का जो एकाधिकार था, वह टूटा; परंतु जहां तक अंतर्वस्तु या उसके उद्देश्य की बात है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वह और मजबूत ही हुई। निश्चित रूप से यह उद्देश्य था जनता को शासित बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक चेतना से निर्मित उसकी संस्कृति का क्षरण करना और उसे औपनिवेशिक शासन के प्रति अनुकूल बनाना।
‘इस प्रकार वर्गों के अस्तित्व वाले समाज में अथवा ऐसी स्थिति में जहां एक राष्ट्र या नस्ल या वर्ग पर दूसरे राष्ट्र या नस्ल या वर्ग का प्रभुत्व है, वहां कोई ऐसी शिक्षा नहीं हो सकती जो किसी निष्पक्ष संस्कृति का प्रसार करे। किसी उत्पीड़क वर्ग अथवा राष्ट्र अथवा नस्ल के लिए शिक्षा उत्पीड़न का उपकरण होती है अर्थात वह मौजूदा समाज व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण होती है, जबकि संघर्षशील वर्ग, नस्ल अथवा राष्ट्र के लिए मुक्ति का उपकरण बन जाती है अर्थात यथास्थिति के सामाजिक रूपांतरण का हथियार बन जाती है। इस तरह के वर्गीय समाजों में दरअसल दो तरह की शिक्षा के बीच भीषण संघर्ष चलता है जो दो परस्पर विरोधी संस्कृतियों का प्रसार करती है और दो परस्पर विरोधी चेतना अथवा विश्वदृष्टि अथवा विचारधाराओं की वाहक हैं।2
जब हम औपनिवेशिक काल के शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टि डालते हैं तो इसे हम और बेहतर ढंग से जान पाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे शिक्षा धीरे-धीरे औद्योगिक जरूरतों एवं अंग्रेजी राज के अनुरूप बनती चली जाती है और अंततः उत्पीड़न एवं मुक्ति दोनों का ही एक प्रमुख औजार बन जाती है। अंग्रेजी राज की आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार से एक ओर जहां पिछले ढाई हजार सालों से गुलाम बना समाज जागृत होता है, तो वहीं उस जागृत समाज को कैसे दबाया जाए, ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा पर आधारित नवीन सांस्कृतिक चेतना को फिर से अंकुरित होने से पहले ही उसे कैसे उखाड़ दिया जाए, यह औपनिवेशिक विचार जड़ जमाने लगा। इसी विचार की अभिव्यक्ति हमें मैकाले के इस कथन में दिखाई पड़ती है –
‘‘मैंने भारत के ओर-छोर का भ्रमण किया है और मैंने एक भी आदमी नहीं पाया, जो चोर हो। इस देश में ऐसी समृद्धि, ऐसे सक्षम व्यक्ति तथा ऐसी प्रतिभा देखी है कि मैं नहीं समझता कि हम इस देश को विजित कर लेंगे, जबतक कि हम इसके सांस्कृतिक एवं नैतिक मेरूदंड को तोड़ न दें। इसलिए मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि हम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति को बदल दें। क्योंकि यदि भारतवासी यह सोचने लगेंगे कि जो विदेशी एवं अंग्रेजी है, वह उनके आचार-विचार से अच्छा व बेहतर है, तो वे अपना आत्मसम्मान एवं संस्कृति खो देंगे और वे एक पराधीन कौम बन जाएंगे, जो हमारी चाहत है।’’ (लार्ड मैकाले का 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में दिए गए वक्तव्य का अंश)
इसी औपनिवेशिक नीति पर चलते हुए सर थामस मुनरो ने 2 जुलाई 1822 को भारतीय शिक्षा पर गहन सर्वेक्षण के आदेश दिये थे। आदेश के साथ जिलाधिकारियों को एक फार्म/प्रपत्र/ भी भेजा गया था। प्रपत्र के जरिए तब पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के नाम, स्कूलों में शिक्षा का समय, मासिक या वार्षिक शुल्क के विवरण और विद्यालयों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के स्रोतों की जानकारी मांगी गयी थी। यह भी पूछा गया था कि क्या विद्यालयों में धर्मशास्त्र, कानून और ज्योतिष जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं? दरअसल, अंग्रेजी सत्ता भारत पर मजबूत शासन चाहती थी। इसके लिए शिक्षा तंत्र पर वास्तविक नियंत्रण की जरूरत थी। इसके लिए पहले से जारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा तंत्र के अध्ययन की आवश्यकता थी। अंग्रेजी राज ने इसीलिए सर्वेक्षण करवाया था। सर्वेक्षण से चौंकाने वाले नतीजे आये। सर्वे का कार्य बाम्बे प्रेसीडेंसी में 1830 तक व मद्रास प्रेसीडेन्सी में 1826 तक हुआ। बंगाल और पंजाब में भी सर्वे का काम हुआ। मद्रास प्रेसीडेंसी के 21 जिलों के सर्वेक्षण में 1094 शिक्षण संस्थांए ‘कालेज’ की हैसियत में थीं। वेद, विधिशास्त्र, तर्कशास्त्र और ज्योतिष अध्ययन के भी आंकड़े उत्साहवर्द्धक थे। सर्वे के अनुसार सभी वर्गाे, जातियों, उपजातियों के हजारों छात्र अध्ययनरत थे। ईसाई मिशनरी (डब्लू एडम) का बंगाल सर्वेक्षण ‘ए रिपोर्ट ऑन दि स्टेट आफ एजुकेशन इन बंगाल’ चर्चा का विषय बना। बंगाल पर एडम की रिपोर्ट कई दफा छपी। 1883 में प्रति विद्यालय एक अध्यापक नाम से इसकी भारी चर्चा हुई। अनेक सर्वेक्षणों के बाद विलियम एडम का निष्कर्ष था कि बंगाल और बिहार के प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्कूल था। बंगाल और बिहार के 150748 गांव में 1 लाख स्कूल थे। बंगाल के प्रत्येक जिलों में कम से कम 100 शिक्षण संस्थाएं थी। मुम्बई प्रेसीडेन्सी और पंजाब के भी निष्कर्ष ऐसे ही थे। देश में लाखों स्कूल थे। वे प्राचीन भारत (सामंती व्यवस्था) की शिक्षा प्रणाली का विस्तार थे। अंग्रेजी राज ने ये स्कूल नहीं चलवाये थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के पूर्व शिक्षा भारत में धर्म तत्व थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति का साधन थी। भारत का धर्म अंध आस्था नहीं है। इसका विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हुआ। गांधीजी ने भी धर्म की शिक्षा को नीति की शिक्षा बताया है। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए।3 यहां धर्म का मतलब नीति है। समाज को ठीक दिशा में ले जाने वाली आचार सारिणी का नाम ‘नीति’ है, इसी की परम्परा का नाम रीति है और रीति वैदिककालीन ‘ऋत’ का ही देशज रूप है।
इसके पश्चात् 1883 ई. के आज्ञा-पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा का आंशिक दायित्व प्राप्त किया। इसके अनुसार कम-से-कम एक लाख की धन-राशि प्रतिवर्ष इस मद में खर्च की जानी थी। लेकिन आज्ञा-पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन-राशि देशी शिक्षा के विकास में खर्च की जाएगी या कि विदेशी शिक्षा के विकास में। फलस्वरूप विवाद उत्पन्न हुआ और 1883 के बाद भी इस विवाद का अंत नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम तथा साधन में निश्चिंतता नहीं बरती गई थी।
संदर्भ:
- कृष्ण कुमार, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, पृष्ठ-13
- न्गूगी वा थ्योंगो, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, पृष्ठ-127
- मोहनदास करमचंद गांधी, हिन्द स्वराज, राजपाल एंड संस, दिल्ली, 2010, पृष्ठ-92